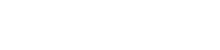लोक परंपराओं और लोक गीतों में वर्ष 1857 के पहले से ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखी और गाई जाने लगी थीं. इनमें अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़ालिम, बेईमान और नाइंसाफ़ बताया गया है.
ख़ासकर प्लासी की ज़ंग में जब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से हारे तभी से काफ़ी लोगों ने शेर लिखे और इसमें उन्होंने विरोध भी किया है.
उर्दू के अलावा खड़ी बोली, भोजपुरी और मगही में तो बहुत कुछ लिखा और कहा गया.
दोनों तरह की बातें हुईं कुछ साहित्य लिखा हुआ मिलता है और लोकगीत कभी लिखित रूप में सामने नहीं आए बल्कि लोग इसे गाया करते थे.
रामग़रीब चौबे नाम के एक साहब थे जिन्होंने बहुत सामग्री जमा की थी.एक दिलचस्प लोककथा है जो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है.
विलियम फ़्रेज़र जो दिल्ली में रेज़िडेंट थे, हिंदू और मुसलमानों से काफ़ी घुल-मलकर रहता था. गाय और सूअर का माँस नहीं खाता थे.
लेकिन उसके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी था. वो काफ़ी अय्याश और ज़ालिम था. उसके जमाने में दिल्ली के आसपास को लोग गाँव छोड़कर जंगलों में चले गए थे. वह लड़कियों का उठवा लेता था.
एक बार फ़्रेजर ने मेवात की रहने वाली सृजन को उठवा लिया था. इस पर सृजन-फ़्रेजर के नाम से मशहूर लोकगीत है.
यह वाकया सन् 1834-35 का है. इससे पता चलता है कि लोकगायक उस दौर में भी कितना जागरूक थे.
ज़ुरैब के बारे में कहा जाता था कि वे सिर्फ़ प्रेम की शायरी किया करते थे लेकिन वर्ष1757 में सिराजुद्दौल की हार के बाद अंग्रेज़ों ने जब अपने पिठ्ठुओं को बंगाल का नवाब बनाया तो उन्होंने जिस तरह हालात को बयाँ किया है, वह गौर करने लायक है.
उनकी एक शायरी है-
समझे न अमीर इनको कोई, न वज़ीर
अंग्रेज़ के कफ़स में है असीर
जो कुछ वो पढ़ाएं सो ये मुंह से बोलें
बंगाले की मैना है ये पूरब के अमीर
यानी बंगाल के नवाब को अंग्रेज़ जो पढ़ाते हैं वो वही बोलते हैं. ये दिखाता है कि उस समय अंग्रेज़ों को लेकर कितनी कठोर प्रतिक्रिया थी.
सन् 1857 से बहुत पहले का बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर है तब वह बादशाह भी नहीं बने थे.
एतबारे सब्र-ए-ताकत हाथ में रखूँ ज़फ़र
फ़ौज-ए-हिंदुस्तान ने कब साथ टीपू को दिया.
इससे ज़ाहिर होता है कि ज़फ़र हिंदुस्तान के राजनीतिक हालात से पूरी तरह वाकिफ़ थे. नहीं तो वे ऐसी शायरी नहीं कर पाते क्योंकि टीपू सुल्तान 1799 में ही युद्ध में मारे गए थे.
लोकसाहित्य में अंग्रेज़ों के ज़ुल्मों की कहानी कही जाती थीं
फ़िरोज बख़्त जो कि शाह आलम के पोते थे अंग्रेज़ों से झगड़कर मुंबई चले गए थे. उन्होंने सन् 1857 में आज़मगढ़ में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें अंग्रेजों के विरोध का कारण आर्थिक शोषण बताया है.
दरअसल 1857 की पूरी लड़ाई ही उर्दू मे लड़ी गई क्योंकि इसमें जो कुछ भी एलान हैं चाहे वह झाँसी की रानी की हों, नाना के हों, बहादुर शाह ज़फ़र के हों या बेगम हजरत महल के हैं वो सब उर्दू में हैं.
इसके अलावा जो भी कविताएं लिखी गईं वे सब उर्दू या खड़ी बोली में हैं.
अवधी, भोजपुरी और मगही में तो बहुत-सी कविताए हैं. बाबू कुंवर सिंह के बारे में भोजपुरी और मगही में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन इसके समय के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है.
जैसे कि मुसहफ़ी का देहांत वर्ष 1824 में हो गया था तो ज़ाहिर है कि उन्होंने इससे पहले ही यह लिखा होगा कि-
जोड़-तोड़ आवे हैं क्या ख़ूब नतारा केतईं
फौज़े दुश्मन को सेबूंहीं लेते हैं सरदार को तोड़
ज़ाहिर है कि यहाँ उनका मतलब सिराजुद्दौला के मीर ज़ाफर के बारे में भी है और टीपू सुल्तान के साज़िद के बारे में भी हैं.
इन चीज़ों से मालूम होता है कि हमारे यहाँ के जागरूक लेखक को इसका अहसास था कि हमारे ऊपर विदेश हुक्मरान आ गया है.
शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, उपाध्यक्ष, काउंसिल फ़ॉर प्रमोशन ऑफ़ लैंग्वेज
(बीबीसी से साभार)